







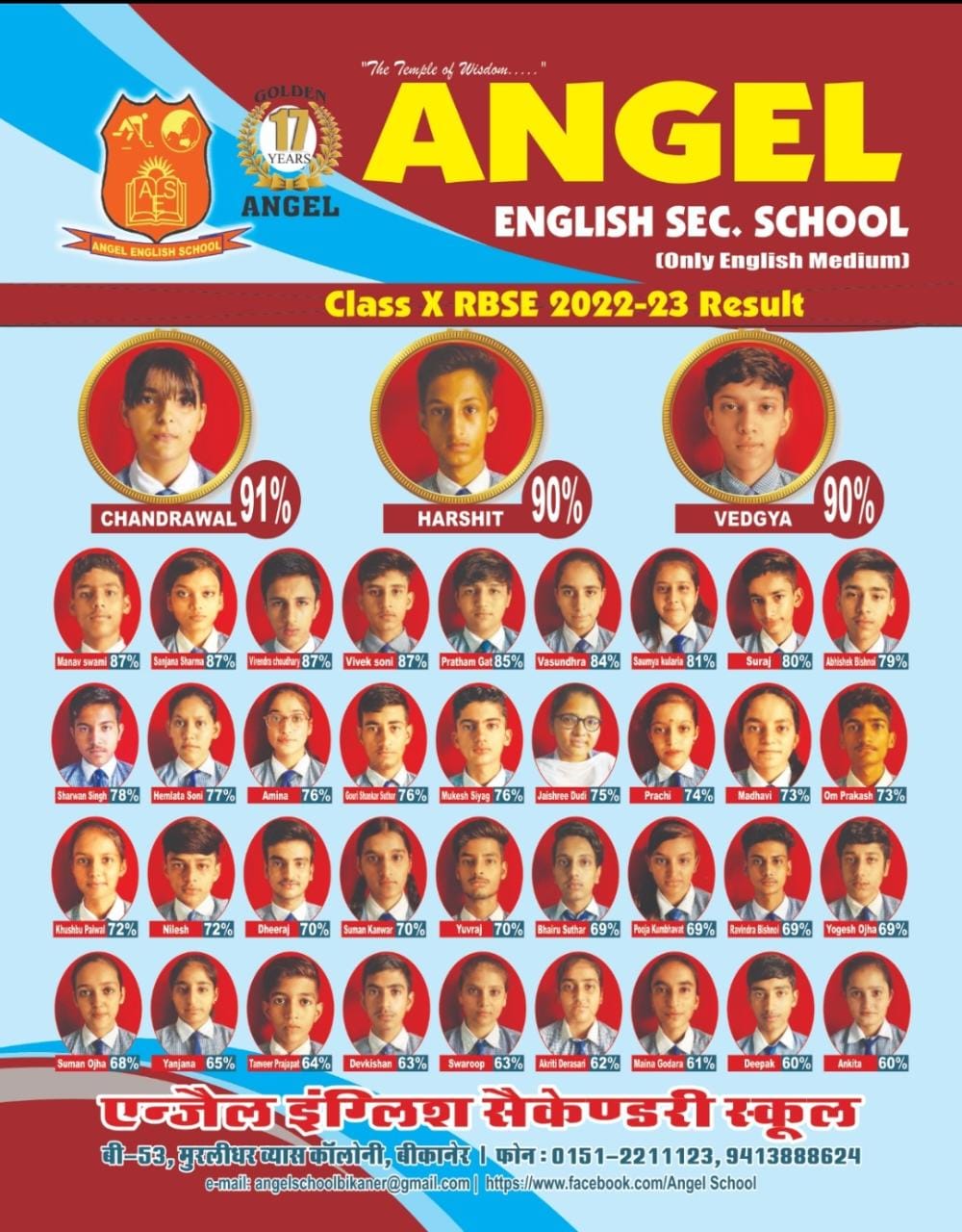

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। हमारा ज्यादातर समय बेकार की बहस में चला जाता है। दिन भर में हम कई बार बहस में उलझ जाते हैं जिसका न कोई लाभ होता है, न कोई निष्कर्ष सामने आ पाता है। कुल मिलाकर आजकल बहस का सीधा सा अर्थ टाईमपास और मनोरंजन तक पहुँच गया है।
टीवी न्यूज चैनलों से लेकर गाँव की चौपालों तक की बात हो या फिर फेसबुक से लेकर दूसरी ढेरों प्रकार की सोश्यल साईट्स, बहस का यह रोग इतना ज्यादा फैलता जा रहा है कि लगता है जैसे इस देश में बहस के सिवा कुछ और बचा ही नहीं है।
राजधानियों से लेकर गांव की पंचायत तक हर कोई भिड़ा हुआ है किसी न किसी तरह की बहस में। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा बहस में रमा हुआ है। भले ही यह बहस उसके काम की हो या न हो। बहस की बदौलत सभी को काम-धंधा मिला हुआ है। बहस कराने वाले भी खुश हैं और बहस करने वाले भी। दोनों किस्मों को टाईमपास का सुनहरा मौका मिल रहा है और तथाकथित लोकप्रियता मिल रही सो अलग।
कोई दुकान-दफ्तर, घर-आँगन, गली-चौराहे, गांव-कस्बे, शहर-महानगर ऐसे नहीं बचे हैं जहाँ किसी न किसी प्रकार की बहस न हो रही हो। ये बहस ही है जो लोगों को अपनी विद्वत्ता, श्रेष्ठता साबित करने और अपने आपको अन्यतम बताने का सर्वोपरि माध्यम बनी हुई है।
जो लोग बहस को लोकप्रियता पाने का जरिया मान बैठे हैं उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बहस से पैदा होने वाली लोकप्रियता अपने आप में बहस का विषय हो जाती है। बहस कुछ समय के लिए लोकप्रियता का भ्रम जरूर दे सकती है लेकिन इससे होने वाला धु्रवीकरण न हमारे हित में होता है, न समाज के।
बात किसी विचार की हो अथवा सूत्रा की, इनकी श्रृंखला का कोई अन्त नहीं होता, यह अपने आप में अनन्त होती है। ‘मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना’ लोक जीवन का वह सर्वाधिक व्यापक फलक है जहाँ वैचारिक मतभेदों और विचारों का बहुमुखी होना स्वाभाविक ही है। फिर बात चाहे कैसी भी हो, इसका कोई अंत नहीं है।
हर व्यक्ति अपनी टाँग ऊँची रखना चाहता है और इसके लिए वह चाहता है कि उसके द्वारा कही बात को सभी स्वीकारें और मानें। और जब टाँग ऊँची रखने की आदत ही पड़ जाए तो हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह स्वभाव सदियों से ग्राम सिंहों का ही रहा है। यही कारण है कि अपनी टाँग ऊँची रखने के आदी लोगों का पूरा का पूरा स्वभाव ही इन श्वानों की तरह ही हो जाता है।
कोई टाँग ऊँची रखने का आदी हो चुका है तो कोई फटे में टाँग अड़ाने का शगल पाले हुए है। और इसी आदत के चलते उन्माद का जो दौर शुरू होता है वह सनक और पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। ‘यथा राजा तथा प्रजा’ का पूरा-पूरा परिपालन करते हुए हम हमारे लोकनायकों और खलनायकों के नक्शे कदम पर चलते हुए बकवासी बहस को जीवन का वह अभिन्न अंग बना डालते हैं जिसके बिना हमारा जीवन नीरस और निरर्थक लगता है। तर्क-कुतर्क भरी बहसें न हों तो हम लोगों को लगता है कि जीवन में कहीं कोई अधूरापन है, कुछ छूटा हुआ रह गया है। बहस का अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। जहाँ मौका मिला, हम शुरू हो जाते हैं। और अब तो ठिकाने की जरूरत भी नहीं रही। अपने पास मोबाईल आ गया है। चाहे जिससे भिड़ जाओ और चलते-फिरते चिल्लाते हुए बहस करनी शुरू कर दो। लोग चाहे कुछ सोचें-समझें। चाहे लोग इसे भौंकना ही कह डालें, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमें तो जीवन जीने के लिए विटामिन से भी सौ गुना ऊर्जा और जीवनीशक्ति यह बहस दे डालती है।
इन सभी प्रकार की बहसबाजियों के बीच सर्वमान्य बात तभी संभव हो पाती है जबकि या तो वह सच्चाई से भरी हो अथवा सभी के स्वार्थों से जुड़ी हुई हो। इंसान का स्वार्थ हो या अहंकार, सभी मामलों में पूर्वाग्रह और दुराग्रहों का होना सामान्य प्रक्रिया है और इसी से जन्म होता है बहसों का।
बहस चाहे कैसी भी हो, क्षणिक स्वीकार्यता और लोकप्रियता को छोड़ दिया जाए तो बहस का रोग हमेशा आदमी की सेहत और जीवन के लिए आत्मघाती ही रहता है। यों देखा जाए तो जो लोग मेधावी और समझदार होते हैं वे बहस और फालतू के बकवास से सर्वथा दूर ही रहते हैं और धीर-गंभीर बने हुए अपने काम में तल्लीन रहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग बहस करते हुए जीवन रस की प्राप्ति करते रहते हैं और इन लोगों के लिए बहस करना दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है जो उन्हें ऐसा टॉनिक देता है जिससे वे स्वर्गीय आनंद और महान सुकून का अहसास करते हैं।
बहस करने के आदी लोग भले ही कितने स्वस्थ और मोटे-तगड़े लगें मगर उनकी सेहत को ठीक नहीं माना जा सकता है। बात-बात में क्रोधित होना, अपनी बात मनवाने के लिए दुराग्रह करना, भौंहें चढ़ाना, आँखें तैरना और दाँत कटकिटाने से लेकर मनोभावों और शरीर की मुद्राओं का बनना-बिगड़ना इस बात को सिद्ध करता है कि बहस करने वाला उत्तरोत्तर मनोरोगी होता जा रहा है।
यही स्थिति सोशल नेटवर्किंग साईट्स पर वैचारिक बहस लिखते रहने के आदी लोगों की हो जाती है जो अपने विचारों की प्रतिक्रिया जानने और इनका जवाब देने दिमाग खपाते हैं और टकटकी लगाए रहते हुए इसी में घंटों गुजार देते हैं। यह भी अपने आप में मनोरोगों को जन्म देने की आरंभिक अवस्था कही जा सकती है।
आजकल टीवी चैनलों ने इस पागलपन को जगर्दस्त हवा दे रखी है। देश में जाने कहाँ-कहाँ से ऐसे-ऐसे लोगों का बहस फोबिया जग गया है जो चैनल खोलो, बहसबाजों की क्रमिक भीड़ हमेशा तैयार। इन्हें कुछ न कुछ बोलना ही है और जनता को सुनना। जोर-जोर से चिल्लाने, भौंकने और झपट्टामार भाव भंगिमाओं के साथ एक-दूसरे पर हावी हो जाने की हमलवार मनोवृत्ति पर कभी रोना आता है और कभी हँसी।
इन तमाम स्थितियों में बातूनी बहसबाजी भरे खर-दूषणों ने ऐसा घातक प्रदूषण फैला रखा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लगता है कोई युद्ध ही हो रहा हो, जिसका शोर सुनते चले जाओ, नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला।
जीवन का कोई सा क्षेत्रा हो, बहस का रोग पालने से बचें। अपनी बात प्रेमपूर्वक पूरे धैर्य के साथ परोस दें। फिर यह प्रयास न करें कि कौन क्या कह रहा है, लिख रहा है या प्रतिक्रिया कर रहा है। वैसे देखा जाए तो जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है, जो लोग संस्कारों से भरे हुए हैं, वे ही बहस की संक्रामक और असाध्य महामारी से मुक्त रहते हैं। जो लोग फालतू के विषयों पर बहस करने के आदी हो गए हैं उनसे बचें और बहस के समय का मार्गान्तरण करते हुए इस समय को रचनात्मक गतिविधियों और समुदाय एवं क्षेत्रा की सेवा में लगाएं।
इससे बहस की छुआछूत भरी महामारी से बचे भी रहेंगे और जीवन में लोकसेवी कर्मों की सुगंध भी पसरने लगेगी। आज बहस से ज्यादा जरूरी है हमारी शक्ति, समय और मेधा का रचनात्मक उपयोग। सरलता से समझ में आ जाए तो ठीक है वरना जीवन भर रोते-चिल्लाते रहो, भौंकते-झपटते और लपकते रहकर अपना अस्तित्व सिद्ध करते रहो, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हमारे ऊपर जाने के बाद हमसे मुक्त होकर सुखी हुए लोग जी भर कर खुशी-खुशी हँसते रहने वाले हैं















